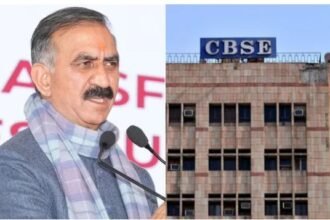उत्तराखंड के कोटद्वार की घटना कोई साधारण खबर नहीं थी। वह एक आईना थी—हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारे दावों का। उस उन्मादी भीड़ के सामने खड़े होकर जब मोहम्मद दीपक ने एक मुस्लिम दुकानदार की जान बचाई, तब उन्होंने सिर्फ़ एक इंसान को नहीं बचाया, बल्कि भारत की उस आत्मा को बचाया, जो कहती है—मुसीबत में मज़हब नहीं, इंसानियत देखी जाती है।
भीड़ का उन्माद डरावना था। नारे, गुस्सा और हिंसा—सब कुछ नियंत्रण से बाहर। ऐसे समय में अधिकांश लोग या तो चुप रहते हैं या सुरक्षित दूरी बना लेते हैं। लेकिन मोहम्मद दीपक ने जोखिम उठाया। उन्होंने ढाल बनकर खड़े होने का फ़ैसला किया। न कोई हथियार, न कोई ताक़त—सिर्फ़ साहस, विवेक और इंसानियत।
यहीं से कहानी का सबसे कड़वा अध्याय शुरू होता है—सिस्टम की भूमिका।
जिस व्यक्ति ने कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ढह जाने से पहले हालात को संभाला, उसी व्यक्ति को बाद में शक की निगाह से देखा गया। जिस दीपक को नागरिक साहस का प्रतीक बनना चाहिए था, वह प्रशासनिक उदासीनता, सामाजिक ट्रोलिंग और नैरेटिव की राजनीति का शिकार हो गया। न कोई स्पष्ट सुरक्षा, न सार्वजनिक समर्थन, न ही यह स्वीकारोक्ति कि अगर ऐसे लोग न हों, तो समाज अराजकता की ओर फिसल जाता है।
यह केवल मोहम्मद दीपक के साथ अन्याय नहीं है—यह एक संदेश है।
संदेश यह कि जब आप नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो सिस्टम अक्सर आपके साथ खड़ा नहीं होता।
मोहम्मद दीपक उन लाखों भारतीयों की आवाज़ हैं, जो संकट की घड़ी में धर्म नहीं पूछते। वे उस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ हिंदू–मुस्लिम, सिख–ईसाई, अमीर–गरीब की दीवारें गिर जाती हैं, और सिर्फ़ इंसान बचाने की प्राथमिकता बचती है। ऐसे लोग टीवी डिबेट्स में नहीं चमकते, लेकिन भारत की नींव इन्हीं पर टिकी है।
दुर्भाग्य यह है कि हमारी व्यवस्था नफ़रत फैलाने वालों से निपटने में जितनी सख़्त दिखती है, उतनी ही धीमी और असहज इंसानियत का साथ देने वालों के प्रति हो जाती है। जब बहादुरी को संरक्षण नहीं मिलता, तो अगला मोहम्मद दीपक शायद आगे बढ़ने से पहले दो बार सोचेगा—और यही सबसे बड़ा ख़तरा है।
आज सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि मोहम्मद दीपक के साथ क्या हुआ।
सवाल यह है कि क्या हम ऐसे भारत को बढ़ावा देना चाहते हैं जहाँ इंसानियत जोखिम बन जाए?
अगर सिस्टम वास्तव में मज़बूत है, तो उसे भीड़ से ज़्यादा भरोसा उन नागरिकों पर करना होगा, जो आग के सामने पानी बनकर खड़े होते हैं। मोहम्मद दीपक कोई अपवाद नहीं हैं—वे वह भारत हैं, जिसे हम खोना नहीं चाहते।
अब फ़ैसला हमारे समाज और सिस्टम को करना है—हम नफ़रत का शोर सुनेंगे या इंसानियत की शांत, लेकिन मज़बूत आवाज़?